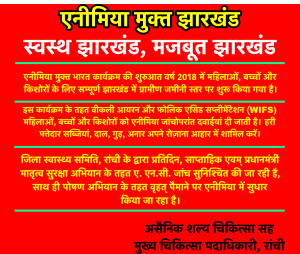आज और कल के सवालों को स्वर देता कथा संग्रह 'खामोशी की आवाज - 3'
जहां तक इस संग्रह में दर्ज कथाओं के पाठन से समझ पाया हूं कि समाज में घटित घटनाओं और परिघटनाओं के साथ-साथ उसकी प्रवृत्तियों, चुनौतियों, संभावनाओं, हार - जीत से आगे जमाने के मिजाज, तेवर, मनोविज्ञान और बदलते समय में आज और कल के सवालों को संबोधित करने तथा उन्हें समझने और सुलझाने के तरीकों में, जिंदगी को बेहतर बनाने और उसे खूबसूरत आयाम देने का काम किया गया है।
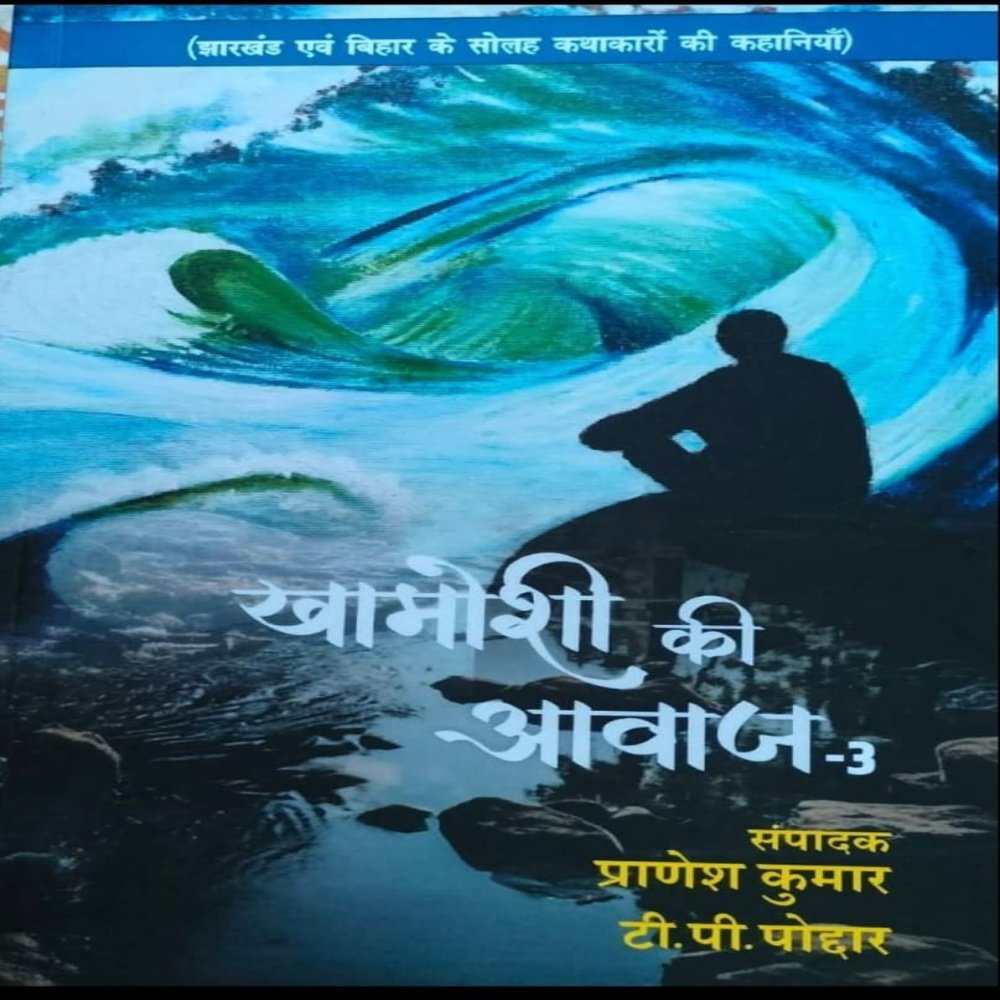
प्रख्यात साहित्यकार कवि स्वर्गीय प्राणेश कुमार एवं टी.पी पोद्दार के संयुक्त संपादन में झारखंड और बिहार के सोलह लब्ध प्रतिष्ठित कथाकारों की सोलह चुनिंदा कहानियों को लेकर 'खामोशी की आवाज - 3' नामक कहानी संग्रह का प्रकाशन किया गया है। यह कहानी संग्रह एक प्रकार से अंतर्मन की खामोशी को तोड़ते हुए समाज के विभिन्न पहलुओं पर सम्यक दृष्टि से विचार कर 'आवाज' बनने का काम करता है। 'खामोशी की आवाज - 3' के संयुक्त संपादक प्राणेश कुमार एवं टीपी पोद्दार दोनों गहरे मित्र रहे हैं । दोनों ने ही संयुक्त रूप में विचार कर यह योजना बनाई कि झारखंड और बिहार के सोलह कथाकारों की सोलह कहानियों को लेकर संग्रह निकाला जाए। दोनों ने बहुत ही मेहनत कर, कथाकारों से संपर्क कर, कहानियां संग्रहित कर संपादन किया। लेकिन संग्रह के प्रकाशित होने के कुछ दिन पूर्व ही भाई प्राणेश कुमार इस दुनिया से अलविदा हो गए। प्राणेश जी के असमय जाने से पोद्दार जी बहुत मर्माहत हुए कि उन्होंने एक गहरे रूप से जुड़े साहित्यकार मित्र को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन टी.पी. पोद्दार जी भी रुकने वाले कहाँ थे। उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ उक्त कहानी संग्रह का प्रकाशन समय पर किया।
लेकिन टी.पी.पोद्दार के मन मस्तिष्क में एक टीस रह गई कि उन दोनों ने जो संयुक्त रूप से कहानी संग्रह निकालने का काम शुरू किया था , संग्रह तो समय पर जरूर आ गया, लेकिन इसके एक प्रमुख योजनाकार प्राणेश कुमार अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस कहानी संग्रह की प्रति उनके हाथों में होती तो कितने खुश होते। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। 'खामोशी की आवाज - 3' से पूर्व इसी श्रृंखला में दो अन्य संग्रह , जो कविता संग्रह हैं, का प्रकाशन भी इसी ' खामोशी की आवाज़ ' सिरीज के अंतर्गत हो चुका है । एक तरह से यह कहानी संग्रह पूर्व के दो संग्रहों का विस्तार है ।
जहां तक इस संग्रह में दर्ज कथाओं के पाठन से समझ पाया हूं कि समाज में घटित घटनाओं और परिघटनाओं के साथ-साथ उसकी प्रवृत्तियों, चुनौतियों, संभावनाओं, हार - जीत से आगे जमाने के मिजाज, तेवर, मनोविज्ञान और बदलते समय में आज और कल के सवालों को संबोधित करने तथा उन्हें समझने और सुलझाने के तरीकों में, जिंदगी को बेहतर बनाने और उसे खूबसूरत आयाम देने का काम किया गया है। इसके साथ ही इस संग्रह में शामिल हर एक कथाकार ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से एक नई बात कहने की कोशिश की है। बात बहुत दूर की नहीं , बल्कि घर परिवार के बनते बिगड़ते रिश्ते, आम आदमी के सपने और संघर्ष की है।
इस संग्रह में शामिल झारखंड और बिहार के ही सोलह कथाकारों की कहानियों को क्यों शामिल किया गया ?इस संदर्भ में जहां तक मेरी दृष्टि जाती है , मैं यही समझ पा रहा हूँ कि बिहार और झारखंड कभी एक ही प्रांत हुआ करता थे। लेकिन झारखंड अलग प्रांत संघर्ष ने इसे दो प्रांत बनने के लिए विवश कर दिया था । बहुत सारे लोग, जो कभी एकीकृत बिहार में रहा करते थे, नौकरी और व्यवसाय के लिए झारखंड में आ बसे थे। उसी तरह बहुत सारे लोग जो पहले झारखंड में रहते थे, नौकरी और व्यवसाय के लिए बिहार में जा बसे थे। दोनों तरफ के लोग इधर-उधर बस तो जरूर गए, लेकिन वे सभी किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े ही रहे हैं। दोनों तरफ के लोगों को अपनी-अपनी जन्मभूमि की टीस जरूर सालती रहती होगी। इस टीस को समझते हुए प्राणेश कुमार और टी.पी. पोद्दार ने बिहार और झारखंड के कथाकारों की कहानियों को लेकर इस संग्रह का प्रकाशन किया। उन दोनों ने एक तरह से अन्तर्मन की इस खामोशी को इस संग्रह के माध्यम से एक नया स्वर प्रदान किया है।
'खामोशी की आवाज - 3' में दर्ज सोलह कहानियां समाज में घटित हो रही उन तमाम घटनाओं का, जिनका सीधा वास्ता घर परिवार से है, उन सबों की परेशानियों, संघर्ष, जन्म भूमि के प्रति लगाव और दुःख को समझने और समझाने का प्रयास है। इस संग्रह की कहानियां खामोश बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी खामोशी को अपनी इन सोलह कहानियों के माध्यम से खुद को एक दूसरे से परिचित कराने का प्रयास करती नज़र आती हैं। इस संग्रह के सभी कथाकार, हिंदी साहित्य की जानी-मानी हस्ती हैं, जिनकी सैकड़ो रचनाएं लाखों करोड़ों पाठकों के बीच दस्तक देती रहती हैं। प्राणेश कुमार और टी.पी. पोद्दार ने इस संग्रह में ऐसी कहानियों को शामिल किया है, जो समाज को एक नई दिशा भी प्रदान कर सके। आज की बदली सामाजिक, राजनीतिक परिस्थिति और आपाधापी भरी जिंदगी में जहां बहुत सारे लोग हताश और परेशान हैं, यहां तक कि कुछ लोग थोड़ी सी परेशानियों के आने भर से आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। प्राणेश कुमार और टी.पी. पोद्दार ने हताशा और परेशानियों से जूझ रहे लोगों को इन कहानियों से प्रेरणा देने का भी काम किया है।
इस संग्रह में बिहार और झारखंड के जिन कथाकारों की रचनाओं को शामिल किया गया है, उनमें सबसे पहला नाम रमणिका गुप्ता, शैलेंद्र अस्थाना, प्रह्लाद चंद्र दास, रतन वर्मा, सुनील सिंह, अनंत कुमार सिंह, डॉ नीरज सिंह, ललन तिवारी, टी.पी. पोद्दार ,जय नंदन, अनवर शमीम, रूपलाल बेदिया, पंकज मित्र, श्याम बिहारी श्यामल, नीलोत्पल रमेश और शांतनु हैं। यहां यह लिखना जरूरी हो जाता है कि इन सोलह कथाकारों में रमणिका गुप्ता और सुनील सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। प्राणेश कुमार और टी. पी. पोद्दार ने रमणिका गुप्ता और सुनील सिंह की एक - एक कहानी को शामिल कर यह बताने का काम किया है कि व्यक्ति इस दुनिया में आता है, फिर एक समय बाद वह इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन उसकी कृतियां जीवित रह जाती हैं। रमणिका गुप्ता और सुनील सिंह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन 'खामोशी की आवाज - 3' कथा संग्रह में उन दोनों की कहानियों को शामिल कर जीवंत करने का भी काम किया गया है। उन दोनों संपादकों ने यह बता दिया कि लेखक कभी मरते नहीं हैं।
इस संग्रह में सबसे पहली कहानी के रूप में रमणिका गुप्ता की कहानी 'परबतिया' शामिल की गई है । यह मेरा परम सौभाग्य है कि उनके साथ कुछ सामाजिक कार्यों में मिलजुलकर करने का अवसर प्राप्त हुआ था। यह कहानी महिला विमर्श, महिला संघर्ष और महिला सशक्तिकरण में विस्तार पाने की कहानी है । रोजी-रोटी की तलाश में पलायन और अपनी जमीन से विस्थापन कैसे आपसी संबंधों को गढ़ता है, इस पर आधारित है। विस्थापन क्या होती है ? परबतिया कैसे इस विस्थापन के खिलाफ उठकर खड़ी होती हैं और अपना वजूद कायम करती हैं ।
इस संग्रह की दूसरी कहानी शैलेंद्र अस्थाना की 'टीस नदी की' दर्ज की गई है। 'टीस नदी की' नाम से ही प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं इस कहानी में एक दर्द है। एक गम है। यह कहानी मुख्यतया कोरोना काल पर आधारित है। यह कहानी तीन मुद्दों के बीच संवाद को आगे बढ़ाती है। और अपने अंदाज में अंजाम तक पहुंचाती है। यह कहानी आदमी की खुदगर्जी, जमाने की उदासीनता, बाजार के मुनाफे की हवस और सत्ता के असंवेदनशील हो जाने की टीस को बताती है।
संग्रह की तीसरी कहानी के रूप में प्रह्लाद चंद्र दास की 'जोगी बाबा का आश्रम' दर्ज की गई है। यह कहानी आस्था और अंधविश्वास के फैलते बाजार, सरकार, व्यवस्था और मीडिया के सहयोग से अवैज्ञानिकता पर जमकर प्रहार करती नजर आती है।
इस संग्रह में चौथी कहानी के रूप में रतन वर्मा की कहानी 'ढोल' को शामिल किया गया है। इस संग्रह में प्रकाशित होने से पूर्व यह कहानी मैं एक पत्रिका में पढ़ चुका हूं । 'ढोल' कहानी एक ऐसी महिला के जीवन संघर्ष को दर्शाते हुए कई सवालों को भी खड़ी करती हैं। एक युवती चलती ट्रेन में गाना गाकर अपनी आजीविका बड़ी मुश्किल चला पाती है। यह कहानी समाज के अंतिम छोर पर धकेल दिए गए लोगों की कहानी है। एक अकेली महिला किस तरह अपनी अस्मिता, स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए कदम कदम पर जूझते और मुकाबला करती हुई आगे बढ़ती है, पर आधारित है।
इस संग्रह की पांचवी कहानी स्वर्गीय सुनील सिंह की 'अपरिचित' को शामिल किया गया है। यह कहानी दो दोस्तों के बीच समय के साथ बदलते रिश्ते, बदलती सोच और बदलते व्यवहार पर आधारित है ।
डॉ नीरज सिंह की कहानी 'जरूरत' अपने शीर्षक के अनुरूप, जरूरत के समय उसकी दशा क्या हो जाती है ? और जब काम सध जाता है, तब उसकी दशा क्या हो जाती है ?इसी पर आधारित है।
इस संग्रह की छठी कहानी टी.पी.पोद्दार की 'रिशु काना' को शामिल किया गया है। यह कहानी तार तार होते मानवीय रिश्ते और मानवीय मूल्य के क्षरण को दर्शाती है।
इसके साथ ही अनंत कुमार सिंह की 'अब और नहीं', ललन तिवारी की 'काला कोट', जय नंदन की 'टेढ़ी उंगली और घी', अनवर शमीम की 'खर्राटें', रूपलाल बेदिया की 'शहर के दाग का दान', पंकज मित्र की चमनी गंझू की मुस्की', श्याम बिहारी श्यामल की 'सीधान्त, नीलोत्पल रमेश की 'बेरंग रिश्ते' और शांतनु की 'इतिहास' कहानी शामिल की गई है। निश्चित तौर पर यह संग्रह मील का पत्थर साबित होगा। प्रत्येक कथाकार की कहानी ने एक नई बात कहने की कोशिश की है।


 Vijay Keshri
Vijay Keshri